
इमेज स्रोत, EPA
जैसे ही संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन (कॉप30) ब्राज़ील में शुरू हुआ, सोशल मीडिया पर जलवायु परिवर्तन को लेकर झूठे और भ्रामक दावे लगातार फैल रहे हैं, जिन्हें लाखों लोग देख चुके हैं.
ऐसे में हम पाँच दावों पर नज़र डालते हैं और बताते हैं कि वे ग़लत क्यों हैं.
दावा: जलवायु परिवर्तन इंसानों की वजह से नहीं हो रहा
ऐसे झूठे दावे लगातार फैल रहे हैं कि इंसान जलवायु को नहीं बदल रहे हैं. ये दावे अंग्रेज़ी, स्पेनिश, रूसी और फ़्रेंच जैसी कई भाषाओं में साझा किए जा रहे हैं.
सच यह है कि पृथ्वी के इतिहास में तापमान बढ़ने और घटने के कई प्राकृतिक दौर आए हैं. इसकी वजहें जैसे ज्वालामुखी विस्फोट या सूरज की गतिविधियों में बदलाव रही हैं.
लेकिन ऐसे बदलाव बहुत लंबे समय में हुए, आम तौर पर हज़ारों या लाखों सालों में.
विश्व मौसम विज्ञान संगठन (डब्ल्यूएमओ) के मुताबिक़, सिर्फ़ पिछले 150 सालों में ही धरती का तापमान लगभग 1.3 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है.
वैज्ञानिकों का कहना है कि इतनी तेज़ी से तापमान बढ़ना कम से कम पिछले कई हज़ार सालों में नहीं देखा गया.
इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज (आईपीसीसी) का कहना है कि यह बदलाव साफ़तौर पर इंसानी गतिविधियों से हो रहा है, जैसे कोयला, तेल और गैस जैसे ईंधनों का जलना.
आईपीसीसी संयुक्त राष्ट्र की एक संस्था है जो दुनियाभर के वैज्ञानिकों को साथ लाकर जलवायु से जुड़ी रिसर्च का आकलन करती है और फ़ैक्ट पर आधारित रिपोर्ट तैयार करती है.

इमेज स्रोत, Getty Images
जीवाश्म ईंधन जलाने से ग्रीनहाउस गैसें, खासकर कार्बन डाइऑक्साइड, हवा में फैलती है. ये गैसें पृथ्वी के चारों ओर एक परत बना लेती हैं, जो अतिरिक्त गर्मी को फँसा लेती हैं और धरती को और ज़्यादा गर्म कर देती हैं.
लंदन के इम्पीरियल कॉलेज की क्लाइमेट साइंटिस्ट जॉयस किमुताई कहती हैं, “जलवायु परिवर्तन मानने या न मानने की बात नहीं है, बल्कि यह सबूतों से साबित होने वाली सच्चाई है.”
“इंसानी गतिविधियों के निशान पृथ्वी की जलवायु प्रणाली के हर हिस्से में साफ़ दिखाई देते हैं.”
दावा: दुनिया ठंडी हो रही है, गर्म नहीं
सोशल मीडिया पर कुछ लोग, जैसे पोलैंड या कनाडा में रहने वाले यूज़र्स, अपने इलाक़ों में सामान्य से ज़्यादा ठंडे मौसम को देखकर कहते हैं कि वैज्ञानिक झूठ बोल रहे हैं और धरती असल में गर्म नहीं हो रही, बल्कि ठंडी हो रही है.
लेकिन यह दावा ग़लत है.
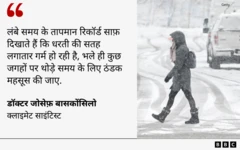
मौसम का मतलब है धरती के वातावरण में कुछ दिनों या हफ़्तों के अंदर होने वाले बदलाव, जबकि जलवायु उन रुझानों और औसत स्थितियों को दर्शाती है जो लंबे समय तक बनी रहती हैं.
फ़िलीपींस के क्लाइमेट साइंटिस्ट डॉक्टर जोसेफ़ बासकोंसिलो कहते हैं, “लंबे समय के तापमान रिकॉर्ड साफ़ दिखाते हैं कि धरती की सतह लगातार गर्म हो रही है, भले ही कुछ जगहों पर थोड़े समय के लिए ठंडक महसूस की जाए.”
विश्व मौसम विज्ञान संगठन के मुताबिक़, 1980 के दशक से अब तक हर दशक पिछली तुलना में ज़्यादा गर्म रहा है, और यह रुझान आगे भी जारी रहने की संभावना है.
संगठन ने बताया कि साल 2024 अब तक का सबसे गर्म साल रहा. इस साल धरती का औसत तापमान 1800 के दशक के अंत की तुलना में करीब 1.55 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा था.

इमेज स्रोत, Getty Images
दावा: कार्बन डाइऑक्साइड पॉल्यूटेंट नहीं है
जो लोग इंसानों की वजह से होने वाले जलवायु परिवर्तन से इनकार करते हैं, वे अक्सर दावा करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड कोई पॉल्यूटेंट नहीं, बल्कि “पौधों का भोजन” है.
बीबीसी को पुर्तगाली और क्रोएशियाई में ऐसे पोस्ट मिले हैं जिनमें कहा गया है कि वातावरण में ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होना प्रकृति के लिए अच्छा ही है.
लेकिन यह सच नहीं है.
पॉल्यूटेंट वह पदार्थ होता है जो पर्यावरण में जाकर ईकोसिस्टम या इंसान की सेहत को नुकसान पहुँचाए.
नासा के मुताबिक़, वायुमंडल में सामान्य स्तर पर मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड धरती पर जीवन के लिए ज़रूरी है. अगर ग्रीनहाउस गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड न हों, तो हमारा ग्रह जीवन के लिए बहुत ठंडा हो जाएगा.
पौधे भी पानी और सूर्य के प्रकाश के साथ कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके ऑक्सीजन और जैविक पदार्थ बनाते हैं, जो धरती पर फ़ूड चेन की बुनियाद हैं.
लेकिन जब वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो वैज्ञानिक इसे “पॉल्यूटेंट” मानते हैं क्योंकि यह नुक़सान पहुँचाने लगता है.

इमेज स्रोत, DANIEL MUNOZ/AFP via Getty Images
विश्व मौसम विज्ञान संगठन के मुताबिक़, साल 2024 में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर अब तक के सबसे ऊँचे स्तर पर पहुँच गया. 1750 में यह लगभग 280 पार्ट्स पर मिलियन (पीपीएम) था, जो अब बढ़कर 423 पीपीएम हो गया है.
वैज्ञानिकों ने यह साबित किया है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की यह बढ़ोतरी इंसानों की गतिविधियों की वजह से है, और इसका सीधा संबंध धरती के बढ़ते तापमान से है. इसका असर ईकोसिस्टम पर पड़ रहा है.
कनाडा की ईकोलॉजिस्ट और कंज़र्वेशन साइंटिस्ट मिशेल कलामांडीन कहती हैं, “जंगलों में आग लगने का ख़तरा बढ़ रहा है, सूखा और बाढ़ फसलों को नुक़सान पहुँचा रहे हैं, और जंगली जानवर अपना घर खो रहे हैं क्योंकि ईकोसिस्टम का संतुलन बिगड़ रहा है.”
इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज का कहना है कि वायुमंडल में ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड से पौधों की वृद्धि थोड़ी बढ़ सकती है, लेकिन यह जलवायु परिवर्तन के नकारात्मक प्रभावों जैसे गर्मी, सूखे और पानी की कमी की भरपाई करने के लिए पर्याप्त नहीं है.
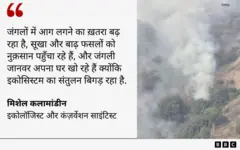
दावा: जंगलों में आग जलवायु परिवर्तन से नहीं, बल्कि लोगों की वजह से लग रही है
जब बड़े पैमाने पर जंगलों में आग लगती है जैसे इस साल अमेरिका, दक्षिण कोरिया और तुर्की में लगी तो सोशल मीडिया पर कई लोग इसका कारण जलवायु परिवर्तन नहीं, बल्कि लोगों की तरफ़ से लगाई गई आग बताते हैं.
ऐसे वायरल पोस्टों में अक्सर वैज्ञानिकों और नेताओं का मज़ाक उड़ाया जाता है, जो इन आग की घटनाओं को जलवायु परिवर्तन से जोड़ते हैं.

इमेज स्रोत, Getty Images
हालांकि यह सच है कि कई बार आग इंसानों की लापरवाही या जानबूझकर किए गए कामों से लगती है, लेकिन इसे केवल एक कारण से जोड़ना “भ्रामक” है.
कोलंबिया की नेशनल यूनिवर्सिटी की साइंटिस्ट डॉक्टर डोलोर्स अरमेंटेरस, जो आग के ईकोसिस्टम पर रिसर्च करती हैं, उनका कहना है, “जंगल की आग को सिर्फ़ एक वजह से जोड़ना बुनियादी तौर पर ग़लत है.”
किसी ख़ास आग को जलवायु परिवर्तन से सीधे जोड़ना आसान नहीं है, क्योंकि इसमें कई कारक भूमिका निभाते हैं जैसे जंगलों का प्रबंधन, मौसम की स्थिति और ज़मीन की बनावट.
फिर भी, यह बात साबित हो चुकी है कि जलवायु परिवर्तन ऐसी परिस्थितियाँ बना रहा है जिनमें जंगलों में आग लगना और फैलना ज़्यादा आसान हो गया है.
इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज (आईपीसीसी) के मुताबिक़, पश्चिमी उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी यूरोप जैसे क्षेत्रों में जलवायु परिवर्तन की वजह से “फ़ायर वेदर” यानी आग के अनुकूल मौसम की घटनाएँ बढ़ गई हैं.
इसमें लंबे समय तक सूखा रहना, अत्यधिक गर्मी और तेज़ हवाएँ शामिल हैं.
ऐसे हालात में अगर किसी भी तरह की चिंगारी चाहे वह प्राकृतिक रूप से बिजली गिरना हो, या मानवजनित आगज़नी या दुर्घटना हो, उसमें सूखी वनस्पति के साथ मिलने से वह गंभीर जंगल की आग का रूप ले सकती है.
डॉक्टर अरमेंटेरस कहती हैं, “सवाल यह नहीं है कि आगज़नी ज़िम्मेदार है या जलवायु परिवर्तन. असल सवाल यह है कि बढ़ती गर्मी और मौसम किस तरह किसी भी आग के सोर्स के प्रभाव को कई गुना बढ़ा देती है, जिससे आज हम इतनी भयानक आग की घटनाएँ देख रहे हैं.”

इमेज स्रोत, LUIS ACOSTA/AFP via Getty Image
दावा: जलवायु ‘इंजीनियरिंग’ की वजह से मौसम असामान्य हो रहा है
सोशल मीडिया पर अक्सर दावे किए जाते हैं कि भारी बारिश, बाढ़ या तूफ़ान जैसे मौसमीय घटनाएं मौसम में की जा रही छेड़छाड़ या ‘जियोइंजीनियरिंग’ के कारण हो रही हैं.
जब पिछले साल संयुक्त अरब अमीरात के दुबई या स्पेन के वेलेंसिया में अचानक आई बाढ़ ने तबाही मचाई, तो बहुत से यूज़र्स ने इन्हें ऐसे ही प्रयोगों का नतीजा बताया.
लेकिन मौसम में बदलाव और जियोइंजीनियरिंग, जो एक-दूसरे से अलग हैं, दुनिया में हो रहे असामान्य मौसम को नहीं समझा सकते.
मौसम को कुछ हद तक बदला जा सकता है. अमेरिकी सरकार की एक रिपोर्ट के मुताबिक़, हाल के वर्षों में चीन, मेक्सिको और भारत समेत 30 से ज़्यादा देशों ने “क्लाउड सीडिंग” तकनीक का इस्तेमाल किया है.
इसमें बादलों में सिल्वर आयोडाइड जैसे छोटे कण छोड़े जाते हैं ताकि उनमें मौजूद जलवाष्प पानी की बूंदों या बर्फ़ के कणों में बदल सके और बारिश या बर्फ़बारी की संभावना बढ़े.

इमेज स्रोत, AFP via Getty Images
भारतीय विज्ञान संस्थान के सेंटर फॉर एटमॉस्फेरिक एंड ओशियैनिक साइंसेज़ के प्रोफेसर गोविंदासामी बाला कहते हैं, “मौसम बदलने की तकनीकें सिर्फ छोटे इलाकों में और थोड़े समय के लिए असर करती हैं. इसलिए ये दुनिया भर में पिछले कई दशकों से हो रहे तेज़ जलवायु बदलावों को नहीं समझा सकतीं.”
वैज्ञानिक मानते हैं कि क्लाउड सीडिंग जैसी तकनीकों के प्रभाव पर बहस हो सकती है, लेकिन ये अकेले किसी बड़ी बाढ़ या व्यापक तूफ़ान की वजह नहीं बन सकतीं.
दूसरी ओर, जियोइंजीनियरिंग का मतलब है, जलवायु को प्रभावित करने के मकसद से पर्यावरण में बड़े पैमाने पर बदलाव करने की कोशिशें.
इसका एक प्रस्तावित तरीका “सोलर रेडिएशन मोडिफ़िकेशन” है, जिसमें वायुमंडल में बारीक कण छोड़े जाते हैं ताकि सूर्य की कुछ रोशनी वापस अंतरिक्ष में परावर्तित हो जाए और धरती ठंडी हो सके.
हालांकि कुछ सीमित और स्थानीय प्रयोग हुए हैं, लेकिन दुनिया के किसी भी हिस्से में सोलर जियोइंजीनियरिंग बड़े पैमाने पर लागू नहीं की जा रही है.
यूके सहित कुछ देशों में हाल के सालों में इस तकनीक पर रिसर्च ज़रूर हुआ है, ताकि यह समझा जा सके कि क्या यह बढ़ती गर्मी को सीमित करने में मदद कर सकती है.
तो फिर दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में हो रहे ऐसे मौसमीय घटनाओं की वजह क्या है? वैज्ञानिकों का कहना है कि जलवायु परिवर्तन के कारण कुछ तरह की मौसम की घटनाएँ, जैसे लू चलना या बहुत ज़्यादा बारिश होना, अब पहले से ज़्यादा बार और ज़्यादा असरदार हो रही हैं.
बीबीसी के लिए कलेक्टिव न्यूज़रूम की ओर से प्रकाशित.
