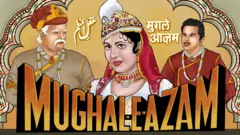
इमेज स्रोत, BBC/Puneet Kumar
-
- Author, वंदना
- पदनाम, सीनियर न्यूज़ एडिटर, बीबीसी न्यूज़
“शहंशाह की बेहिसाब बख़्शिशों के बदले में एक कनीज़ जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर को अपना ख़ून मुआफ़ करती है.”
फ़िल्म मुग़ल-ए-आज़म में वजाहत मिर्ज़ा के लिखे इस डायलॉग में एक तरफ़ हैं बादशाह अकबर और दूसरी तरफ़ उनके दरबार में नाचने वाली कनीज़ अनारकली.
आज से 65 साल पहले 5 अगस्त 1960 को रिलीज़ हुई हिंदी फ़िल्म मुग़ल-ए-आज़म ऐसे संवादों, बेहतरीन गानों और भव्य दृश्यों से भरी पड़ी है.
यहां तक कि जब 2006 में, 46 साल बाद, ये फ़िल्म पाकिस्तान में रिलीज़ हुई तब भी इसका प्रीमियर काफी भव्यता से किया गया था.
कराची में शाही दरबार जैसे थिएटर में लगी मुग़ल-ए-आज़म

इमेज स्रोत, BBC/Puneet Kumar
वरिष्ठ पत्रकार ख़ालिद फ़रशोरी उन लोगों में शुमार हैं, जिन्हें कराची में उस प्रीमियर में बुलाया गया था.
उस दिन को याद करते हुए ख़ालिद फ़रशोरी बताते हैं, “कराची में थिएटर में इतनी भीड़ थी कि कई फ़ोटोग्राफ़र, रिपोर्टर अंदर नहीं आ सके थे और नाराज़ लोग वहां विरोध तक करने लगे थे. फ़िल्म देखने का इतना क्रेज़ था कि लोग बड़े स्तर पर सिफ़ारिशें लगवा रहे थे.”
“निशात सिनेमा को जैसे किसी शाही दरबार में तब्दील कर दिया गया था. मेहमानों का स्वागत करने वाले भी शाही लिबास में थे. शो के बाद परोसा गया खाना भी रॉयल अंदाज़ में पेश किया गया. फ़िल्म देखने आए लोगों को पान और कहवा परोसा गया.”
इस फ़िल्म के बनने की कहानी समझने के लिए दशकों पीछे लौटना होगा.
दिलीप कुमार और मधुबाला के साथ तो इस फ़िल्म की शूटिंग 1951 में शुरू हुई, जबकि असल में इसकी पहली शूटिंग 1945 में ही शुरू हो चुकी थी.
निर्देशक के. आसिफ के उस मुग़ल-ए-आज़म में अनारकली का किरदार नरगिस निभा रही थीं.
शहज़ादे सलीम की भूमिका में अभिनेता डीके सप्रू थे और अभिनेता चंद्रमोहन अकबर की भूमिका निभा रहे थे.
फ़िल्म की शूटिंग काफ़ी धूमधाम से शुरू हुई और कई गाने भी रिकॉर्ड कर लिए गए.
बंटवारे ने बदल दी मुग़ल-ए-आज़म की कहानी

इमेज स्रोत, Manjul Publishing House
इस मुग़ल-ए-आज़म को बनाने के लिए जिस किस्म की दौलत, टीम, कलाकार और इंतज़ाम चाहिए थे, उसे पूरा करने के लिए निर्माता शिराज़ अली हकीम ने 1945 में अपनी पूरी तिजोरी खोल दी. इस शूटिंग के लिए उन्होंने बॉम्बे टाकीज़ को के. आसिफ़ के हवाले कर दिया.
लेकिन फिर ख़बर आई कि भारत का बंटवारा होने वाला है और शूटिंग रुक गई. फ़िल्म में पैसा लगाने वाले शिराज़ अली हकीम सब कुछ बेच कर पाकिस्तान चले गए.
जब 1951 में फ़िल्म की शूटिंग दोबारा शुरू हुई तो तकरीबन सब कुछ बदल चुका था.
शुरुआती मुग़ल-ए-आज़म में सलीम का रोल कर रहे अभिनेता डीके सप्रू तब तक साइड हीरो का रोल निभाने लगे थे.
अकबर, अनारकली, सलीम सब बदल गए…

इमेज स्रोत, Manjul Publishing House
ख़ैर जब 1951 में फ़िल्म का काम दोबारा शुरू हुआ तो अकबर का किरदार निभा रहे चंद्रमोहन की मौत हो गई. अभिनेता हिमालयवाला शुरुआती मुग़ल-ए-आज़म में दुर्जन का रोल कर रहे थे, लेकिन 1947 में वो भी पाकिस्तान चले गए थे.
सिर्फ़ दुर्गा खोटे एकमात्र कलाकार थीं जो शुरुआती और बाद की मुग़ल-ए-आज़म दोनों में रहीं.
इसे किस्मत कहिए या कुछ और लेकिन के. आसिफ़ को मुग़ल-ए-आज़म की स्क्रिप्ट दोबारा लिखनी पड़ी और तब उन्होंने उसी दिलीप कुमार को बतौर सलीम लिया जिन्हें वो कई साल पहले ठुकरा चुके थे.
हालांकि, 1945 वाली असल मुग़ल-ए-आज़म की नरगिस अब 1951 में अनारकली का रोल नहीं करना चाहती थी. अपनी अनारकली तलाशने में के.आसिफ़ को सबसे ज़्यादा दिक्कत हुई.
अख़बारों में और स्क्रीन पत्रिका में इश्तेहार के बावजूद उन्हें अनारकली नहीं मिली. ये तलाश मधुबाला पर जाकर ख़त्म हुई जो उस वक़्त दिलीप कुमार के साथ रिश्ते में थीं.
दिलीप कुमार जब मुग़ल-ए-आज़म के लिए हुए थे रिजेक्ट

इमेज स्रोत, BBC/Puneet Kumar
यहां ये जानना दिलचस्प है कि 1945 में जब फ़िल्म शुरू हुई थी तो दिलीप कुमार को के.आसिफ़ ने सलीम के लिए रिजेक्ट कर दिया था.
1945 में दिलीप कुमार को मुग़ल-ए-आज़म में न लेने की कहानी दिलीप कुमार की आत्मकथा ‘दिलीप कुमार: द सबस्टांस एंड द शेडो’ में लिखी है.
सितारा देवी के.आसिफ़ की पहली पत्नी थीं और दिलीप कुमार से उनका गहरा रिश्ता था. तब 1944 में आई दिलीप कुमार की ज्वार भाटा फ्लॉप हो चुकी थी.
सितारा देवी के हवाले से किताब में लिखा गया है, “आसिफ़ ने दिलीप कुमार के बारे में सुन रखा था. जब वो मिलने आए तो मेरे सामने एक ऐसा नौजवान था, जिसकी शख़्सियत शहाना (राजसी) थी. चेहरे पर चौंधिया देने वाली नूर की चमक और अंदाज़ में नफ़ासत थी. इसमें कोई शक़ नहीं कि आसिफ़ प्रभावित हुए थे. लेकिन आसिफ़ ने कहा कि मुमकिन है जब मैं दस साल बाद सलीम-अनारकली पर दोबारा स्क्रिप्ट लिखूं, तब शायद उसे सलीम के किरदार के लिए चुन लूं क्योंकि दिलीप में शहाना शान तो है, लेकिन अभी वो इस रोल के लिए तैयार नहीं.”
हामिद करज़ई जब बोले प्यार किया तो डरना क्या
जब आख़िरकार ये फ़िल्म 1960 में बनकर तैयार हुई तो ये सिर्फ़ भारत में ही नहीं बल्कि भारत से बाहर भी कई देशों में बहुत लोकप्रिय हुई.
माजिद नुसरत 1984 में अफ़ग़ानिस्तान छोड़ने से पहले वहीं पले बढ़े थे और अभी बीबीसी की मॉनिटरिंग सर्विस के साथ जुड़े हुए हैं.
वो बताते हैं, “मैंने मुग़ल-ए-आज़म उस वक़्त के एकमात्र अफ़ग़ान टीवी चैनल पर देखी थी. मुझे आज भी अच्छी तरह से याद है कि मैं ‘प्यार किया तो डरना क्या’ गाना देखकर मुग्ध हो गया था.”
“अफ़ग़ान संस्कृति में ये गाना इतना रच बस गया था कि एक बार पूर्व राष्ट्रपति हामिद करज़ई ने अपनी स्पीच में भी इसका इस्तेमाल किया था. जब उनसे भारत में पूछा गया था कि पाकिस्तान के साथ नाज़ुक रिश्तों के बीच अफ़ग़ानिस्तान-भारत के नज़दीकी संबंध को वो कैसे देखते हैं, तो हामिद करज़ई ने हंसते हुए कहा -प्यार किया तो डरना क्या. उनकी यह टिप्पणी सुनकर पूरे हॉल में ज़ोरदार तालियां गूंज उठीं.”
“मेरे अंकल राशिद हिंदी सिनेमा और मुग़ल-ए-आज़म के इतने बड़े फ़ैन थे कि उन्होंने पाकिस्तान के ज़रिए भारत जाने की भी कोशिश की थी, कि शायद उन्हें कोई रोल मिल जाए.”
बड़े ग़ुलाम अली इस तरह फ़िल्म में गाने को तैयार हुए

इमेज स्रोत, NAQI ALI KHAN
बंटवारे से पहले जब फ़िल्म शूट हुई थी, तो उसमें संगीत अनिल बिस्वास ने दिया था, जो उस समय शीर्ष पर थे. लेकिन 1951 में जब दोबारा शूटिंग शुरू हुई, तो यह ज़िम्मेदारी नौशाद ने संभाली.
गानों की बात हो रही है तो यहाँ ‘प्रेम जोगन बन के’ गीत का ज़िक्र ज़रूरी है, जिसे बड़े ग़ुलाम अली ख़ान ने गाया था. वो आमतौर पर फ़िल्मों के लिए गाते नहीं थे.
करीब पांच मिनट का यह गाना तानसेन उस जादुई लम्हे के दौरान गाते हैं, जब अनारकली और सलीम रात को तन्हाई में मिलते हैं.
सफ़ेद पंख से अनारकली (मधुबाला) के होठों को सहलाते सलीम (दिलीप कुमार) का यह सीन हिंदी सिनेमा के सबसे रूमानी दृश्यों में से एक गिना जाता है, जहां बेहद महीन और मखमली अंदाज़ में इज़हार-ए-मोहब्बत किया जा रहा है.
राजकुमार केसवानी लिखते हैं कि बड़े ग़ुलाम अली ख़ान की इस गीत की रिकॉर्डिंग के बारे में नौशाद ने कुछ यूं बताया है, “मैंने के.आसिफ़ से पूछा कि क्या आपके हिसाब से रिकॉर्डिंग हो रही है. तो आसिफ़ ने कहा कि मुझे गीत लव सीन पर फ़िल्माना है तो गले में और नर्मी चाहिए. ख़ान साहब ने सुना तो नाराज़ हो गए. कहने लगे अब रिकॉर्डिंग नहीं होगी पहले मुझे फ़िल्म दिखाइए ताकि मैं समझ सकूं कि मुझे क्या करना है.”
“ख़ान साहब ने फ़िल्म के दृश्य देखे तो उनमें ग़ुम हो गए. बार बार कहते-अमां कितनी ख़ूबसूरत है. ख़ान साहब ने रिहर्सल की. कहने लगे इस शर्त पर गाऊंगा कि फ़िल्म चलती रहे. फ़िल्म चलती रही और ख़ान साहब गाते रहे. गाने का पूरा सिक्वेंस जादू भरा है. मधुबाला के हुस्न का जादू अभी ख़त्म नहीं होता है कि ख़ान साहब के क़मायतखेज़ छोटे छोटे अलाप नया जादू पैदा करते हैं.”
“अभी आप इससे उबरने भी न पाएं कि के.आसिफ़ जादुई सफ़ेद पंख सलीम के हाथ में थमा देते हैं. इसके बाद पर्दे पर जो चमत्कार होता है उसे निहारते-निहारते न जाने कितनी पीढ़ियाँ निहाल हो चुकी हैं.”
मुग़ल-ए-आज़म फ़िल्म जितनी मक़बूल हुई, उसमें बेशक शकील बदायूँनी के गीतों और नौशाद के संगीत का बड़ा योगदान रहा.
भारतीय सैनिक भी जुड़े थे मुग़ल-ए-आज़म से
करीब-करीब 10 साल में बनी ये फ़िल्म न जाने कितनी ही दुश्वारियों से होकर गुज़री है.
के.आसिफ़ एक-एक शॉट के लिए बेहतरीन से बेहतरीन सेट, लिबास, कलाकार लेकर आते थे. युद्ध वाले दृश्य फ़िल्माने के लिए भारतीय सेना के जवान और टेक्नीशियन लाए जाते थे जो ज़मीन के नीचे बारूद बिछाकर धमाके करते थे.
शीश महल का सेट बनाने के लिए फ़िरोज़ाबाद से आग़ा शिराज़ी और कारीगरों को बुलाया गया था. आग़ा शिराज़ी के पिता 20वीं सदी में ईरान से भारत आए थे और शीश महल बनाते थे.
इस बेहिसाब खर्च और सालों-साल चली शूटिंग से फ़िल्म के फ़ाइनेंसर शापूरजी पालोनजी मिस्त्री कई बार बेहद खफ़ा भी हो जाते थे और फ़िल्म बंद होने के कगार पर आ जाती थी. लेकिन शापूरजी पालोनजी ने के.आसिफ़ का साथ नहीं छोड़ा.
फ़िल्म के सेट पर बड़े बड़े लोगों का आना-जाना लगा रहता था जिसमें इटली के मशहूर फ़िल्मकार रोज़लिनी भी शामिल थे.
शाही अंदाज़ में हुआ प्रीमियर

इमेज स्रोत, X/NFAI
बहुत मुश्किलों से मुकम्मल हुई मुग़ल-ए-आज़म जब 1960 में रिलीज़ हुई तो इसका प्रीमियर भी शाही अंदाज़ में मुंबई के मराठा मंदिर में किया गया. मुग़ल-ए-आज़म के सिनेमेटोग्राफ़र आर.डी. माथुर सजे धजे हाथी पर फ़िल्म का प्रिंट लेकर आए थे.
झालर वाले रेश्मी कपड़े पर प्रीमियर का न्योता छप कर तैयार हुआ था और ख़ास रंगीन टिकटें छपवाई गई थीं जिन पर अकबर, अनारकली और सलीम की फोटो थीं.
थिएटर के बाहर सुंदर बगीचा बनाया गया था, थिएटर के अंदर मुलायम गलीचा, पुश बैक सीटें और ए.सी. था. बाहर लेडीज़ टॉयलेट में मुफ़्त में परफ़्यूम और मेकअप का सामान मौजूद रहता था जिसमें लिपस्टिक और पाउडर सब शामिल था.
1960 में मुग़ल-ए-आज़म पाकिस्तान में रिलीज़ नहीं हुई थी लेकिन पाकिस्तान से लोग वीज़ा लेकर हिंदुस्तान ये फ़िल्म देखने आते थे.
‘दास्तान-ए-मुग़ल-ए-आज़म’ में राजकुमार केसवानी लिखते हैं कि जब मराठा मंदिर को चलाने वाले गोलचा सेठ को पता चला तो उन्होंने पाकिस्तानी पासपोर्ट वाले लोगों के लिए लाइन में लगने के बजाए सिनेमा हॉल के अंदर ही टिकट लेने का इंतज़ाम कर दिया था.
फ़िल्म के प्रीमियर पर पाकिस्तान से शिराज़ अली हकीम को भी बुलाया गया जिन्होंने दिल खोल कर पैसा लगाकर 1945 में मुग़ल-ए-आज़म की नींव रखी थी.

इमेज स्रोत, BBC/Puneet Kumar
दिलचस्प बात ये है कि इसी दौरान 1958 में पाकिस्तान में फ़िल्म अनारकली रिलीज़ हुई, जिसमें मुख्य रोल में नूरजहां थीं.
लेखक राजकुमार केसवानी अपनी किताब दास्तान-ए-मुग़ल-ए-आज़म में लिखते हैं, “गीतकार तनवीर नक़वी ने शुरुआती मुग़ल-ए-आज़म के लिए चार गीत लिखे थे. लेकिन जब फ़िल्म फिर से शुरू हुई तो के.आसिफ़ ने इन गीतों का इस्तेमाल नहीं किया.”
पाकिस्तानी फ़िल्म अनारकली में तनवीर नक़वी के दो गाने इस्तेमाल हुए जो उन्होंने मुग़ल-ए-आज़म के लिए लिखे थे और इन्हें गाया नूरजहाँ ने. जैसे ये गाना ‘कहाँ तक सुनोगे, कहाँ तक सुनाऊँ, हज़ारों ही शिकवे हैं, क्या क्या सुनाऊँ.’
‘आवाज़ दे कहां है’ जैसे मशहूर गाने लिखने वाले तनवीर नक़वी भी बंटवारे के बाद पाकिस्तान में बस गए थे.

इमेज स्रोत, BBC/Puneet Kumar
इस दौरान कई दोस्तियां और रिश्ते टूटे
मुग़ल-ए-आज़म पर शाहरुख़ ख़ान ने डॉक्यूमेंट्री बनाई थी जिसमें के.आसिफ़ की पोती हया के.आसिफ़ ने उन्हें इसेन्ट्रिक जीनियस (विलक्षण प्रतिभावान) कहा था.
मुग़ल-ए-आज़म की शूटिंग के दौरान ही के.आसिफ़ और फ़िल्म में बहार का रोल करने वाली अभिनेत्री निग़ार सुल्ताना का इश्क़ भी परवान चढ़ा. लेकिन फ़िल्म के दौरान ही ये रिश्ता टूट भी गया.
दरअसल के.आसिफ़ ने निग़ार से शादी के बावजूद दिलीप कुमार की बहन से चोरी-छिपे शादी कर ली थी. इससे सख़्त नाराज़ दिलीप कुमार ने आसिफ़ से सारे रिश्ते तोड़ लिए और फ़िल्म के प्रीमियर पर भी नहीं गए.
और ये बात तो जगज़ाहिर है कि फ़िल्म की शूटिंग के दौरान ही असल ज़िंदगी के अनारकली और सलीम यानी मधुबाला और दिलीप कुमार का रिश्ता ख़त्म हो चुका था.
ज़िंदा है मुग़ल-ए-आज़म की दास्तां

इमेज स्रोत, Getty Images
ये अजीब इत्तेफ़ाक था कि फ़िल्म ख़त्म होते-होते असल ज़िंदगी के रिश्ते मोहब्बत के बजाय बेबसी और अदावत में बदल चुके थे.
जबकि मुग़ल-ए-आज़म बनने की कहानी और इस फ़िल्म दोनों की बुनियाद बेइतहां मोहब्बत पर टिकी हुई थी.
जैसा कि अकबर बने पृथ्वीराज कपूर फ़िल्म के आख़िरी सीन में अनारकली से कहते हैं, “अनारकली जब तक ये दुनिया क़ायम रहेगी तुम लफ्ज़-ए-मोहब्बत की आबरू बनकर ज़िंदा रहोगी.”
ठीक वैसे ही, जैसे मुग़ल-ए-आज़म को बनाने का नामुमकिन-सा लगने वाला आलीशान ख़्वाब आज भी ज़िंदा है.
दर्जी से निर्देशक बने के.आसिफ़ की ज़िद की कहानी आज भी सुनाई जाती है और दशकों बाद भी मुग़ल-ए-आज़म के किस्से पीढ़ी दर पीढ़ी ज़िंदा है.
बीबीसी के लिए कलेक्टिव न्यूज़रूम की ओर से प्रकाशित
