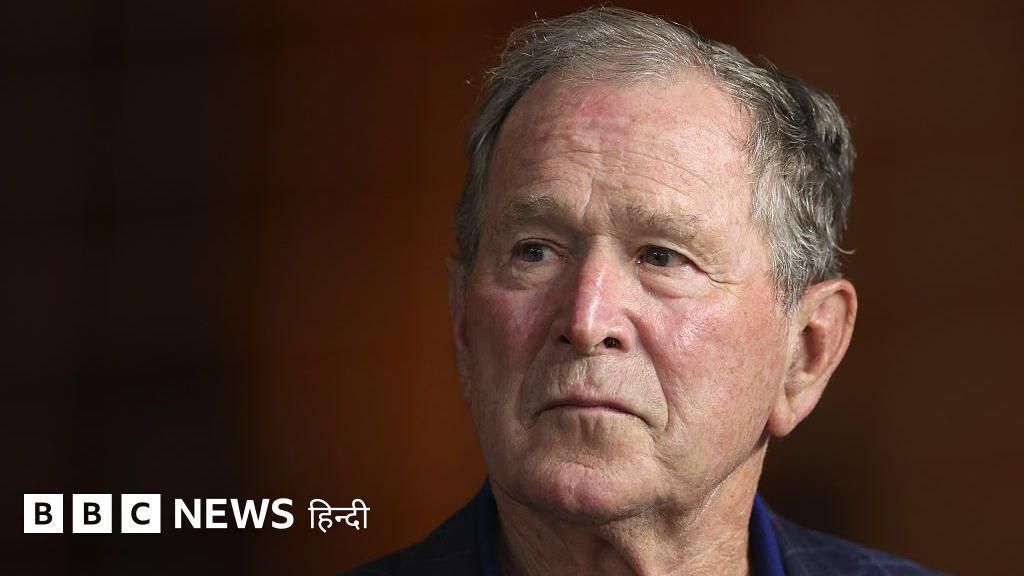इमेज स्रोत, Getty Images
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जब इस साल मई महीने में देश के पूर्व राष्ट्रपतियों के हस्तक्षेप करने की नीतियों की कड़ी आलोचना की थी तो दुनिया भर में इस पर ख़ूब चर्चा हुई.
उन्होंने 2003 में इराक़ पर हुए विवादास्पद अमेरिकी हमले की ओर इशारा करते हुए कहा था, ”आख़िर तथाकथित ‘राष्ट्र-निर्माताओं’ ने जितने देश बनाए, उससे कहीं ज़्यादा देशों को तबाह कर दिया.”
उन्होंने कहा, ”दखल देने वालों ने उन जटिल समाजों में दखल दिया, जिनके बारे में उनकी कोई समझ नहीं थी.”
ये बातें उन्होंने सऊदी अरब की राजधानी रियाद की यात्रा के दौरान कही थीं. कई विश्लेषकों ने उनके इस बयान को इस बात का संकेत माना था कि कम से कम ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में अमेरिका का मध्य-पूर्व में दखल अतीत की बात हो जाएगी.
लेकिन इन बयानों के महज एक महीने बाद ही अमेरिका ने ईरान के तीन परमाणु ठिकानों पर हमला किया. इस तरह अमेरिका, ईरान और इसराइल के युद्ध में घुस गया.
इस हमले के ज़रिये अमेरिका और इसराइल ने ईरान की परमाणु चाहत को ख़त्म करने की कोशिश की.
हमले के तुरंत बाद ट्रंप ने कहा, ”हमारा मक़सद ईरान के यूरेनियम संवर्द्धन की क्षमता को ख़त्म करना और आतंकवाद को समर्थन देने वाले दुनिया के सबसे बड़े देश से पैदा परमाणु ख़तरे को रोकना था.”
लेकिन इतिहास गवाह है कि जब भी पश्चिमी देशों ने विदेशों में “समस्या का समाधान” करने के लिए दख़ल दिया तो अक्सर चीज़ें योजना के मुताबिक़ नहीं हुईं.
लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस में मध्य-पूर्व की राजनीति और अंतरराष्ट्रीय संबंधों के प्रोफ़ेसर और लेबनानी-अमेरिकी लेखक फ़वाद गर्गेस कहते हैं कि 1940 के दशक के अंत से ही अमेरिका मध्य-पूर्व की राजनीति में दख़ल देता रहा है.
“व्हाट रियली वेंट रॉन्ग: द वेस्ट एंड द फेल्योर ऑफ डेमोक्रेसी इन द मिडिल ईस्ट” नाम की किताब के लेखक गर्गेस ने कहा, ”ईरान के ख़िलाफ़ अमेरिका के हालिया हवाई हमले उसकी इस नीति का स्पष्ट उदाहरण है.”
आइए देखते हैं कि अमेरिका ने किन देशों में दख़ल दिया और इसके क्या नतीजे हुए.
ईरान में तख़्तापलट
1953 में ईरानी सेना के एक तख़्तापलट ने देश में लोकतांत्रिक रूप से चुने गए प्रधानमंत्री मोहम्मद मोसादेग़ को हटा दिया. इस काम में अमेरिका और ब्रिटेन ने ईरानी सेना का साथ दिया था.
मोसादेग़ इस वादे के साथ दो साल पहले ही सत्ता में आए थे कि वो ईरान के विशाल तेल भंडारों का राष्ट्रीयकरण करेंगे.
लेकिन इसके साथ ही अमेरिका और ब्रिटेन को संभावित कम्युनिस्ट ख़तरा दिखा.
दूसरे विश्व युद्ध के बाद अमेरिका और ब्रिटेन दोनों ईरान के तेल पर बुरी तरह निर्भर थे.
पहले इसे शाह महमूद रज़ा पहलवी के समर्थन में जनता के विद्रोह के तौर पर पेश किया गया.
इस विद्रोह को अमेरिका और ब्रिटेन दोनों की ख़ुफिया एजेंसियों का समर्थन था.

इमेज स्रोत, Getty Images
साल 2000 में तत्कालीन अमेरिकी विदेश मंत्री मैडलिन अलब्राइट ने खुले तौर पर कहा था कि उस तख़्तापलट में अमेरिका का हाथ था.
फिर 2009 में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने काहिरा में दिए अपने एक भाषण में उस घटनाक्रम में अमेरिका की भूमिका की बात मानी थी.
फिर 2013 में उस तख़्तापलट के 60 साल बाद अमेरिकी ख़ुफिया एजेंसी सीआईए ने कुछ दस्तावेज़ प्रकाशित किए, जिनमें पहली बार उसने उस तख़्तापलट में अपनी इस भूमिका को स्वीकार किया.
प्रोफ़ेसर गर्गेस का मानना है कि अमेरिका और ईरान के बीच मौजूदा टकराव की जड़ें भी इसी गोपनीय हस्तक्षेप से जुड़ी हैं.
वो कहते हैं, ”ईरानियों ने वैध और लोकतांत्रिक तरीक़े से चुने गए प्रधानमंत्री को हटाकर एक क्रूर तानाशाह यानी ईरान के शाह को देश का शासक बनाने के लिए अमेरिका को कभी माफ़ नहीं किया.”
वो कहते हैं, ”ईरान में आज जो अमेरिका विरोधी भावना है, वह इसलिए कि वहाँ की राजनीतिक सत्ता का मानना है कि अमेरिकी हस्तक्षेप की वजह से ही ईरानी राजनीति की दिशा बदल गई है.”
प्रोफेसर गर्गेस इस बात की ओर भी ध्यान दिलाते हैं कि अमेरिका ने मिस्र के राष्ट्रपति गमाल अब्देल नासिर की नीतियों को भी प्रभावित करने और उनकी राष्ट्रवादी परियोजना की दिशा बदलने की कोशिश की लेकिन इसमें ज़्यादा कामयाबी नहीं मिली.
अफ़ग़ानिस्तान में कट्टर इस्लामी ताक़तों का समर्थन
1979 में सोवियत रूस की सेना ने अफ़ग़ानिस्तान पर हमला किया ताकि एक साल पहले सत्ता में आई कम्युनिस्ट सरकार को समर्थन मिल सके.
लेकिन उसे जल्दी ही एक प्रतिरोधी इस्लामी आंदोलन का सामना करना पड़ा. इसे मुज़ाहिदीन के नाम से जाना जाता है.
ये समूह कम्युनिस्ट सरकार का विरोध करने वाले इस्लामी जिहादी चरमपंथियों से बना था. इसे अमेरिका, पाकिस्तान, चीन और सऊदी अरब समेत कई अन्य देशों का समर्थन हासिल था.
शीत युद्ध के दौरान अफ़ग़ानिस्तान को सबसे अधिक हथियार और धन मुहैया कराने वाले देशों में अमेरिका शामिल था. अमेरिका ये सब इसलिए कर रहा था कि ताकि अफ़ग़ानिस्तान में सोवियत रूस के मक़सद को नाकाम किया जा सके.

इमेज स्रोत, Getty Images
वर्षों बाद सार्वजनिक किए गए दस्तावेज़ों, पत्रकारों की जांच और गवाहियों से ये बात सामने आई कि अमेरिका ने सोवियत संघ को अफ़ग़ानिस्तान में एक ऐसे जाल में फंसाने की कोशिश की थी, जो ज़िंदगियों और संसाधनों की भारी कीमत मांगता था. ठीक ऐसा ही हाल अमेरिकी सेना का वियतनाम युद्ध में हुआ था.
अमेरिका के इस मिशन को ऑपरेशन साइक्लोन कहा गया. उस समय की मीडिया रिपोर्टों में इसे “सीआईए के इतिहास का सबसे बड़ा गुप्त ऑपरेशन कहा गया.”
उस समय के अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने तो कुछ जिहादी नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल को ओवल दफ़्तर में भी बुलाया था.
1988 में, जेनेवा समझौते के बाद और लगभग अफ़ग़ानिस्तान में एक दशक के लंबे कब्जे के आख़िर में सोवियत नेता मिख़ाइल गोर्बाचेव ने अफ़ग़ानिस्तान से सोवियत सेनाओं को वापस बुलाना शुरू किया.
आख़िरकार 1989 की शुरुआत में सोवियत सैनिकों ने अफ़ग़ानिस्तान छोड़ दिया.
लेकिन इसके बाद अफ़ग़ानिस्तान अलग-अलग गुटों में बँट गया. सोवियत रूस के समर्थन के बगैर वहां सरकार का टिके रहना मुश्किल हो गया.
इसी अशांत समय के बीच एक नया एक नया चरमपंथी समूह उभरा. जिसे तालिबान कहा जाता था. इसके सदस्य शरीयत क़ानून की एक कठोर व्याख्या में विश्वास करते थे.
इसके कई नेता सोवियत क़ब्ज़े के ख़िलाफ़ मुजाहिदीन आंदोलन में हिस्सा ले चुके थे. इन्हें अमेरिका समेत कई देश हथियार देते थे.
इसी तरह सोवियत-अफ़गान युद्ध ख़त्म होने के बाद इसमें शामिल पूर्व लड़ाकों ने अल-क़ायदा नामक संगठन बनाया ताकि इस्लामी संघर्ष को अफ़ग़ानिस्तान से बाहर भी फैलाया जा सके.
तालिबान ने इस संगठन और इसके नेता ओसामा बिन लादेन को अपने देश में पनाह दी, जहां से उन्होंने 11 सितंबर 2001 को अमेरिका पर हमले की योजना बनाई.
अलाबामा यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस में मध्य-पूर्व अध्ययन के प्रोफ़ेसर वालिद हज़बन कहते हैं कि शीत युद्ध के दौरान अमेरिका के ज़्यादातर हस्तक्षेपों को मध्य-पूर्व में संतुलन बनाए रखने की कोशिश के तौर पर देखा जा सकता है.
उन्होंने बीबीसी से कहा, ”अमेरिका का मक़सद उन सभी राजनीतिक ताक़तों का विरोध करना था जो उसके और उसके सहयोगियों के हितों के ख़िलाफ़ थीं.”
प्रोफ़ेसर हज़बन का कहना है कि 1990–1991 के खाड़ी युद्ध में अमेरिका के नेतृत्व वाला हस्तक्षेप इसका एक उदाहरण है.
उन्होंने कहा, “यह इराक़ का कुवैत पर आक्रमण का जवाब था. कुवैत की संप्रभुता बहाल कर दी गई और शीत युद्ध ख़त्म होने के बाद अमेरिकी नीति निर्माताओं और क्षेत्रीय नेताओं के बीच साझे ज़रूरतों को पूरा करने के तरीक़ों पर चर्चा हुई.”
हालांकि प्रोफे़सर हज़बन कहते हैं कि इसके बाद जब अमेरिका में बिल क्लिंटन का दौर आया तो अमेरिका ने एक नया रुख़ अख़्तियार किया.
उन्होंने कहा, “इसका मक़सद एक ऐसा सुरक्षा ढांचा तैयार करना था जो अमेरिकी हितों और क्षेत्रीय व्यवस्था बनाने के उसके नज़रिये पर खरा उतर सके.”
वो कहते हैं, “इसमें एक तो मध्य-पूर्व में शांति प्रक्रिया और दूसरे अरब-इसराइल संबंधों के सामान्य बनाने पर ध्यान देना शामिल था. ताकि सभी अरब देश अमेरिका और इसराइल के साथ तालमेल बिठा सकें. दूसरी ओर, ईरान और इराक़ को सैन्य तरीक़ों और प्रतिबंधों के ज़रिए नियंत्रित करना भी इसका हिस्सा था.”
कई बार अमेरिकी हस्तक्षेपवाद के साथ-साथ इसराइल को मिला समर्थन भी चलता रहा है, जिसे अमेरिकी नेताओं ने ”बिना शर्त के अटल समर्थन” किया था.
दूसरे विश्व युद्ध के बाद से इसराइल अमेरिका से सबसे अधिक विदेशी सहायता प्राप्त करने वाला देश रहा है, जिसे हर साल अरबों डॉलर की मदद दी जाती है.
तालिबान को काबू करने के लिए अफ़ग़ानिस्तान पहुंचे
अक्टूबर 2001 में अमेरिका ने अफ़ग़ानिस्तान पर हमले का नेतृत्व किया. उसका कहना था कि यह क़दम तालिबान को अफ़ग़ानिस्तान से बाहर करने, लोकतंत्र को समर्थन देने और 11 सितंबर के हमलों के बाद अल-क़ायदा से पैदा ख़तरे के ख़ात्मे के लिए उठाया गया था.
अमेरिका ने बड़ी तेज़ी से देश की राजधानी काबुल पर कब्जा कर लिया.
अफ़ग़ानिस्तान में 2003 से नेटो सैनिक भी मौजूद थे. वो वहां लड़ाइयों में भागीदारी कर रहे थे और अफ़ग़ान सुरक्षा बलों को ट्रेनिंग भी दे रहे थे.
तीन साल बाद एक नई अफ़ग़ान सरकार सत्ता में आई लेकिन तालिबान के खू़नी हमले जारी रहे.

इमेज स्रोत, Getty Images
2009 में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अफ़ग़ानिस्तान में और सैनिक भेजने का एलान किया, जिससे कुछ समय के लिए तालिबान को पीछे धेकलने में कामयाबी मिली. लेकिन ये स्थिति ज़्यादा दिनों तक नहीं रही.
साल 2001 के बाद 2014 सबसे ख़ूनी साल साबित हुआ. नेटो ने वहाँ अपना मिशन समाप्त कर दिया और सुरक्षा की ज़िम्मेदारी अफ़ग़ान सेना को सौंप दी.
इसके बाद तालिबान ने और अधिक क्षेत्रों पर क़ब्ज़ा कर लिया.
अगले साल तालिबान ने अपनी ताक़त बढ़ाना जारी रखा और आत्मघाती हमलों का एक सिलसिला शुरू किया.
उन्होंने काबुल में संसद भवन पर हमले किए और राजधानी के अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास एक और हमले की जिम्मेदारी ली.
आख़िरकार, अप्रैल 2021 में, बाइडन प्रशासन ने अफ़ग़ानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी के फ़ैसले पर मुहर लगा दी. ठीक 20 साल बाद जब अमेरिका के नेतृत्व में यहां हमला हुआ था.
ये एक विवादास्पद फ़ैसला था, जिसकी वजह से अफ़ग़ानिस्तान तेजी से तालिबान के हाथों में चला गया.
इस घटना की तुलना 1975 में दक्षिण वियतनाम में हुई घटनाओं से की जाने लगी.
एक पूर्व अफ़ग़ान अधिकारी ने नाम नहीं छापने की शर्त पर बीबीसी को बताया, ”अमेरिकी सेना की वापसी के साथ ही तालिबान के हाथ बड़ी तादाद में हथियार और दूसरे साजो-सामान लगे. इनमें से ज़्यादातर अमेरिकी पैसों से ख़रीदे गए थे.
2023 की एक संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट बताती है कि तालिबान ने अपने स्थानीय कमांडरों को जब्त किए गए अमेरिकी हथियारों का 20 फ़ीसदी रखने की अनुमति दी थी.
इसके चलते ब्लैक मार्केट में इन हथियारों की ख़रीद-फ़रोख़्त बढ़ गई.
इराक़ पर हमला
अगस्त 1990 में, इराक़ के तत्कालीन राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन के नेतृत्व में इराक़ी सेना ने कुवैत की सीमा पार कर हमला कर दिया, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए. कुवैती सरकार को सऊदी अरब में निर्वासित होना पड़ा.
कई लोगों के लिए ये घटना मध्य-पूर्व के इतिहास में एक लंबे और उथल-पुथल भरे दौर की शुरुआत थी.
इराक़ को कई चेतावनियां दी गईं. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने कुवैत पर हमले के ख़िलाफ़ एक प्रस्ताव भी पारित किया.
फिर दूसरे विश्वयुद्ध के बाद सबसे बड़े सैन्य गठबंधन ने 17 जनवरी 1991 को कुवैत से इराक़ी सेनाओं को हटाने के लिए अपना अभियान शुरू किया.
इस सैन्य गठबंधन का नेतृत्व अमेरिका कर रहा था और इसे ब्रिटेन और सऊदी अरब मदद कर रहे थे.
इसके बाद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने प्रस्ताव नंबर 687 पारित किया. इसमें कहा गया कि इराक़ सामूहिक विनाश के अपने सभी हथियार नष्ट करे.
परमाणु, जैविक और रासायनिक हथियार के साथ ही लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों के लिए सामूहिक विनाश के हथियार जैसे शब्द का इस्तेमाल किया गया.

इमेज स्रोत, Getty Images
साल 1998 में इराक़ ने संयुक्त राष्ट्र हथियार निरीक्षकों के साथ सहयोग करना बंद कर दिया.
इसके बाद 2001 में न्यूयॉर्क स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और पेंटागन पर हुए हमलों के बाद, तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू. बुश ने इराक़ पर हमले बनाने की योजना शुरू की.
बुश ने इराक़ के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन पर सामूहिक विनाश के हथियारों को जमा करने और इनका निर्माण जारी रखने का आरोप लगाया.
उन्होंने कहा कि इराक़, ईरान और उत्तर कोरिया के साथ मिलकर ‘शैतान की धुरी’ का हिस्सा बन गया है.
साल 2003 में तत्कालीन अमेरिकी विदेश मंत्री कोलिन पॉवेल ने संयुक्त राष्ट्र को बताया कि इराक़ ने जैविक हथियार बनाने के लिए “मोबाइल प्रयोगशालाएं” बनाई हैं.
लेकिन 2004 में उन्होंने ख़ुद ये स्वीकार किया कि उनके पास इसके समर्थन में मौजूद सबूत इतने पुख्ता नहीं हैं.
ब्रिटेन,ऑस्ट्रेलिया और पोलैंड ने इराक़ पर अमेरिका के इस हमले में साथ दिया. लेकिन जर्मनी, कनाडा, फ़्रांस और मैक्सिको जैसे कई देशों ने इसका विरोध किया.
बीबीसी के अंतरराष्ट्रीय संपादक जेरेमी बोवेन के मुताबिक़ ये हमला इराक़ और उसके लोगों के लिए एक आपदा साबित हुआ. इसने इराक़ को दशकों तक अराजकता में झोंक दिया.
2023 में इस हमले के 20वें साल में उन्होंने अपने विश्लेषण में लिखा,” ओसामा बिन लादेन और जिहादी चरमपंथियों की विचारधारा को नष्ट करने के बजाय, 2003 में शुरू हुई अराजकता और क्रूरता ने जिहादी हिंसा को और बढ़ा दिया.”
इस हमले का एक और नतीजा ये हुआ कि अल-क़ायदा ने ख़ुद को खड़ा करना शुरू किया और आगे चलकर ये स्वयंभू इस्लामिक स्टेट यानी आईएसआईएस में तब्दील हो गया.
2003 के हमले में कितने इराक़ी मारे गए इसका सटीक आंकड़ा नहीं है.
हालांकि, “इराक बॉडी काउंट (IBC) प्रोजेक्ट के मुताबिक़ 2003 से 2022 तक 2,09,982 इराक़ी नागरिकों की मौत हुई. आईबीसी आक्रमण के बाद मारे गए नागरिकों की गिनती के लिए बना था.
प्रोफेसर हज़बन का कहना है कि अब ज़रूरत इस बात की है कि अमेरिका को क्षेत्रीय स्तर पर शांति प्रयासों का समर्थन देना चाहिए.
उन्होंने कहा,”अमेरिका के वैश्विक हित बेहतर ढंग से तभी पूरे हो सकते हैं, जब यह क्षेत्र (मध्य-पूर्व) साझा सुरक्षा की समझ की ओर बढ़े. अमेरिका और उसके सहयोगियों की भारी सैन्य शक्ति के ज़रिये कोई व्यवस्था थोपने की कोशिश नहीं होनी चाहिए.”
बीबीसी के लिए कलेक्टिव न्यूज़रूम की ओर से प्रकाशित